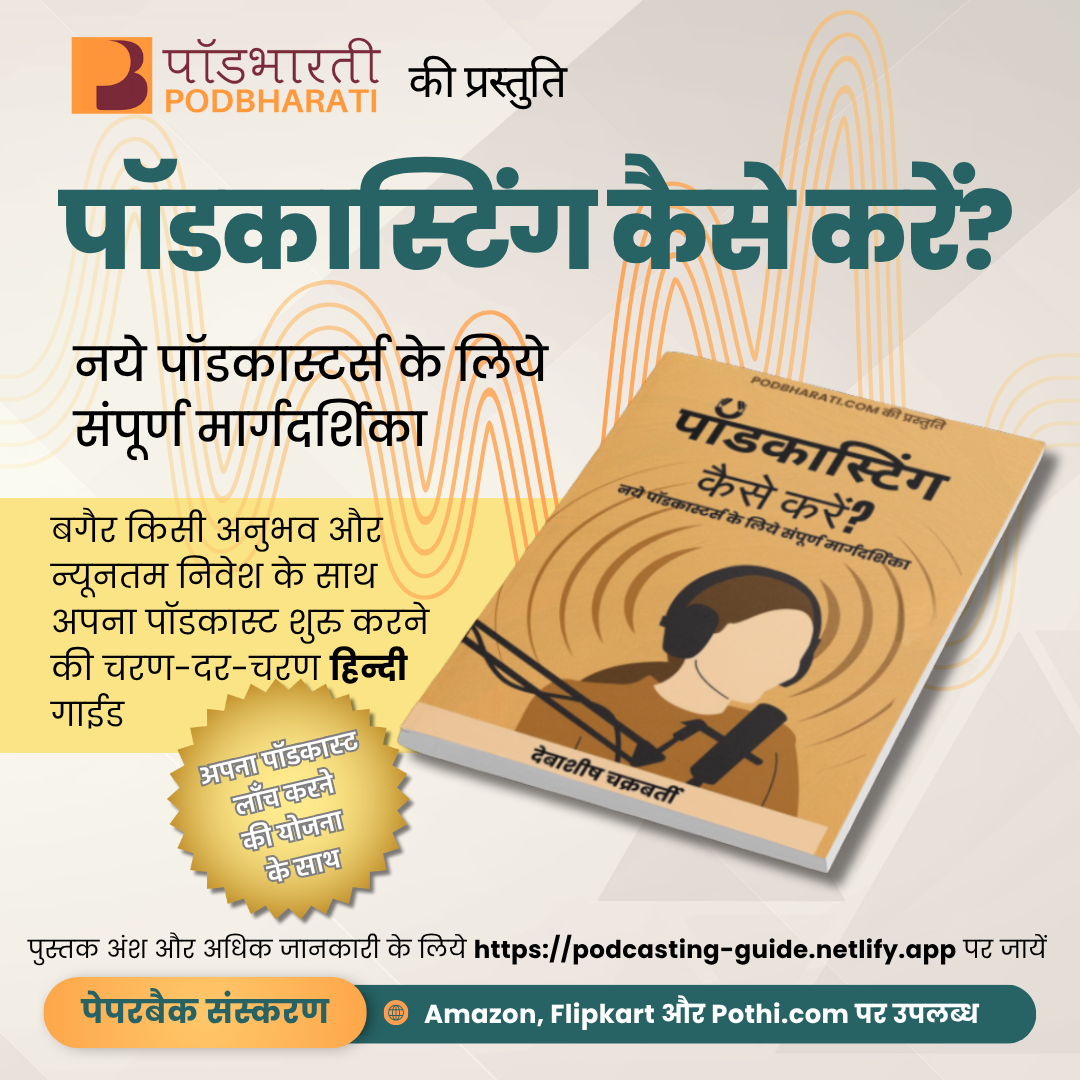वक्त की सूई को जरा पीछे की ओर मोड़ा जाए, बहुमंजिली फ्लैट्स के वक्त से पहले स्वतंत्र मकानों के वक्त में, या फिर उससे भी पहले जब मकान अपने दिल में बड़ा सा आंगन बसाए हुआ करते थे यूँ कहे तो आंगन ही मकानों का दिल होते, वे ही धड़कते। आंगन ही सुर होते, वे ही सरगम। चाहे कितने कमरे हों, सारा घर आंगन में ही चहचहाया करता आंगन में बर्तन-कपड़े धुलते, आंगन में ही पापड़-बड़ियाँ सूखते, आंगन में घर की बहु-बेटियाँ चूड़ियाँ छमकातीं, नई नवेली की पैंजनियाँ छनछनातीं। यहीं पर गर्मी की रातों में चारपाइयाँ बिछतीं, इन्हीं चारपाइयों में न जाने कितनी कहानियाँ जनम लेतीं। सर्दी की दोपहरी आँच भी इसी आंगन में दी जाती। आँगन में ही पड़ोसियों से गप्पबाजी होती, बच्चे खेलते। यही नहीं, हर त्यौहार की पदचाप भी यहीं सुनी जाती।
अब होली आती तो आंगन में न जाने कब से ही पापड़ बड़ियाँ सूखने लगतीं। नई कोरी धोतियों को टेसु के रंग में रंग कर अबरक छिड़क सुखाया जाता। फिर पन्द्रह दिन पहले से गोबर की सिकरियाँ तैयार की जातीं…गोल-गोल चपटी बीच में छेद वालीं उन सबको रस्सी में पुरो कर मालाएँ बनाईं जातीं, फिर उन्हें खूब सुखाया जाता। पूरे पन्द्रह दिन पहले से ही होली का चौक पुरना शुरु हो जाता। होली का चौक कोई ऐसा वैसा तो होता नहीं, बकायदा अबीर गुलाल से पूरा जाता, बड़ी करछुल को रख चुटकी से दबा एक समान आकृति तैयार होती। हर रोज चौक का आकार बढ़ता जाता यानी कि पहले दिन पाँच करछुल का चौक, तो दूसरे दिन सात का, फिर नौ का… बस इसी तरह रंगबिरंगा चौक आंगन को घेरता जाता। अंततः इतना बड़ा बन जाता कि मनों लकड़ियों पर होलिका दहन की तैयारी की जा सके। इसी मौके पर तो पूरा कुनबा जुटता, इतना बड़ा कि आंगन खिलखिला उठता।
होली का सम्बन्ध रंगों से तो था पर बड़े मधुर रंगों से…दो चार दिन पहले से पकवान बनना शुरु हो जाते, गुझिया, पापड़, मीठे गुड़ के सेव, नमकपारे, काँजी के बड़े…न जाने कितनी – कितनी मिठाइयाँ। होली से ऐन पहले पीली दपदपाती धोती पहन माईं होली पूजन के लिए खड़ी होतीं तो कितनी सुन्दर लगा करतीं थीं। रंग भी तो टेसु के ही खेले जाते…टेसु में प्रीत जो होती है। फिर होलिका पूजन होता, पुरोहित जी को आना पड़ता। खास तौर से दहन का कार्य घर के पुरुष करते, किंतु औरतें होली की परिक्रमा करती सुहाग की भीख मांगतीं। होलिका मैय्या से कुँवारी होलिका क्या पाती होगी सुहाग दान…लेकिन महिलाओं के दिल में भय तो भर ही जाता, बिनब्याही होलिका का शाप न लगे…वे परिक्रमा करतीं, जलती आग पर जल छिड़कतीं, मीठे से पूजन करतीं, “हे होलिका मैय्या, रक्षा करना!”
होलिका दहन के बाद गुलाल तो छिड़का जाता किंतु रंगों की फुहार के लिए अगले दिन धुलंडी का इंतजार किया जाता। धुलंडी के दिन आंगन का क्या कहना, कहीं लाल रंग तो कहीं पीला, कही हरा तो कहीं नीला… पूरा आंगन दपदपाने लगता, रंगो का कोलाज आंगन से उतर कर मन में घर बना लेता।
आँगन? पुरातन कथाओं के नायक .. परी कथाओं की परियाँ .. बस वैसा ही लुप्त होता शब्द… आँगन…आँगन बीते दिनों की बातें बन गया… आँगन ही क्यों उसकी गोबरी चमचमाहट पर बिखरीं गोकुल की आकृतियाँ, भाई दूज के भाई बहन की गाथाएँ…बाती दीवट के चावल से मंडे माँडने…होली का अबीर…गुलाल से दमकता चौक… सिकरियाँ…होली दहन…और न जाने क्या-क्या। न जाने क्यों, उसके साथ उल्लास भी पथरा गया…रस सीठा हो गया…
माई की मोड़ी न जाने कब बड़ी हो गई। बेटी से बहु और बहु से माँ। लम्बा सफर है, पर पार हो गया। उसके साथ ही बढ़ती गई उसकी बेटियाँ भी बड़ी कोशिश की उसने कि आँगन की छटा पूजा की कोठरी में चली आए, दीवाली के दीवट, नरक चतुर्थी का दीवला, करवा चौथ की कथा भीत से उतरी तो छपी तस्वीर पर रुकी और वहाँ से भी उतरी तो बस कहानी में ही रह गई। फिर न जाने कैसे बेटियाँ करवा चौथ का इंतजार करने लगीं, गुलगुले-पूरी के लिए, दीए की कथा के लिए, दीवाली को सजाने लगीं। पूजा होती घर के सामने छोटी रंगोली में, घी के पाँच दीयों में, दीवार पर सजी कतार पर…राखी को सजाने लगी…पाप्पा की कलाई पर… माँ की चूड़ियों पर…
त्योहार का रंग बदला, स्वाद भी…पर महक नहीं। खास तौर पर बेटियों के लिए। बेटियों की छनकाहट ने मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि हर भाव के रूप रंग कैसे बदलते हैं? पूरे मोहल्ले में केवल अपने घर में दीए जलते देख आँखें भर आती…हर दीवाली की साँझ को एक उदास चिड़िया आ कर कंधे पर बैठ जाती। लेकिन बेटियों ने तो यही गंध पाई है बचपन से इसलिए उनकी खिलखिलाहट मुरझाती नहीं।
फिर भी यह कोशिश रही कि त्यौहार के दिन किसी न किसी मेहमान को घर पर बुला लिया जाए। थोड़ी सी भीड़-भाड़ रहे, जरा सी रौनक बिखर जाए और इस सुदूर प्रान्त में भी बकायदा होली-दीवाली मनती रही, त्यौहार खिसकते रहे। पच्चीस बरस बीत गए, बड़ी बेटी शादी के बाद ससुराल चली गई, छोटी इंजीनियरिंग के लिए होस्टल में। अब बचे हैं हम दो… हमारे दो से जुदा होने के गम में पिघल-पिघल कर जमते से।
होली आई है… अकेली होली… हम दोनों अकेले हैं। चौबीस-पच्चीस बरस पहले इस अकेलेपन के लिए कितना तरसते थे दोनों, कितना थक जाते थे गृहस्थी के भार से। लेकिन नहीं, यह अकेलापन नहीं। यहाँ तो सन्नाटा गरज-गरज कर बह रहा है। कितना शोर है इस सन्नाटे में, कितनी थकावट है इस अकेलेपन में। युवाओं के लिए अकेलापन आनन्द है तो प्रौढ़ों के लिए संगीत रहित शोक।
गुझिया बनानी है? किसके लिए…बच्चियाँ तो हैं नहीं…यहाँ कोई मेहमान आता नहीं…पड़ोसी झाँकते भी नहीं…महानगरीय संस्कृति वाला नगर है यह, बिना फोन किए कोई किसी के घर नहीं आता। कोई दूसरी मिठाई? किसके लिए?
“तुम कुछ मत करो.. बेटियाँ तो हैं नहीं जो तुम्हारी मदद कर देतीं, मैं बाजार से लड्डू ले आता हूँ,” प्रदीप भी काफी निर्लिप्त हैं। आखिर पूजा का हवन तो होना ही है। हाँ, हवन तो होगा…चौक भी पूरा जाएगा…लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कर्म निपटाया जा रहा हो…निर्लिप्त…निर्मोह…हो कैसे? आंगन तो पूजा की कोठरी के दरवाजे पर कुछ फुट जमीन समा गया है। होलिका चार इंच के हवन कुंड में जल जाएगी।
यहाँ होली मनाता ही कौन है? यहाँ तो लोगों का इस “मूर्खता” के प्रति आक्रोश है…इसलिए काम से छुट्टी भी नहीं। पूजा करनी है तो आफीस से आने के बाद ही ठीक है। शाम को हवन किया, भगवान पर चुटकी भर गुलाल छिड़का, फिर आ कर टीवी के सामने दोनों बैठ गए टीवी के पर्दे पर चित्रहार जैसा ही कोई प्रोग्राम.. रंगों से सराबोर चेहरे.. इधर सोफे पर हम दोनों एकदम सूखे… सामने तश्तरी पर रखे सूखते लड्डू।
यह भी एक होली है… भोपाल की होली से अलग…बच्चियों की होली से भिन्न… होली ही क्यों… न जाने कितने त्यौहार चुपचाप खिसक जाते हैं कालनिर्णय रसोईघर की भीत पर टंगा-टंगा। सब त्योहारों के नाम कान में बुदबुदाता रहता है.. मन मामा के आँगन में उस त्यौहार को मना आता है… बस हो गया बच्चियाँ जब पास थी तो पूछा करतीं, “माँ क्या होता है गणगौर? नागपंचमी किसे कहते हैं? बसन्त पंचमी का नाम तो सुना है पर होता क्या है उस दिन?” कैसे बताती…होली, दीवाली, करवा चौथ, भाईदौज मनाना सिखा दिया, यही कम है क्या? हाँ, उन्होंने परिवेश से भी कुछ त्यौहार सीखे…ओणम…विषु…और क्रिसमस।
उस दिन ओणम के पास बिटिया का खत आया।
“माँ ओणम मनाया जा रहा होगा न! मुझे पायसम की खुशबू आ रही है।”
मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी खुशबू और बच्चियों की खुशबू में अन्तर है लेकिन एक बात समान है कि उनके पास भी बचपन की मुट्ठी भर यादें हैं.. जगमगते जुगनुओँ सी।
सामने मेज पर लड्डू सूख रहे हैं…रंग में सराबोर है…हम दोनो नहीं …हमारे मन।